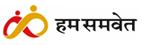दुनिया तो बदलेगी, लेकिन कैसी यह हम नहीं जानते
वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन की कलम से कोरना वायरस की दहशत और इसके बाद दुनिया में होने वाले परिवर्तन की संभावना का विश्लेषण।

कोरना वायरस की दहशत इस हद तक फैली हुई है कि धनी और मध्य वर्ग के लोग फिलहाल अपनी जान बचा लेने से आगे या उससे इतर की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का जो हाल है या समाज के गरीब एवं मेहनतकश तबकों पर जैसी मार पड़ी है, वह फिलहाल उनकी और मेनस्ट्रीम मीडिया की चिंता से बाहर है। कम-से-कम ये बात पूरी तरह अपने देश पर लागू होती है। आखिर एक नया वायरस इतना घातक क्यों साबित हो रहा है, इस प्रश्न पर अपने देश में शायद ही कोई सार्थक चर्चा हुई है। फिलहाल बनी परिस्थिति के बीच आज की आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था एवं हावी विचारों का क्या योगदान है, इस पर भारत में कोई बहस खड़ी नहीं हुई है। यह इसका भी एक नतीजा है कि भारत सरकार अपनी तमाम नाकामियों के बावजूद किसी कठघरे में खड़ी नजर नहीं आती। नतीजतन, उसके लिए हालात पर काबू पाने, उससे उबरने, और पीड़ित लोगों को वास्तविक राहत देने की कोई मजबूरी नहीं बनी है।
मगर ऐसा सभी जगहों पर नहीं है। यूरोप और अमेरिका में जो बहसें चल रही हैं, उस पर गौर करें, तो वहां आज पिछले चार दशक से अपनाई गई आर्थिक नीतियां कठघरे में खड़ी नजर आती हैं। ये वो दौर है, जब पुर्तगाल या स्पेन जैसे इक्का-दुक्का देशों को छोड़ दें, तो ज्यादातर देशों में दक्षिणपंथी या धुर-दक्षिणपंथी दलों/ नेताओं की सरकारें हैं। मगर उन सरकारों ने कोरोना वायरस के संकट का मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाए हैं, वो उनकी बुनियादी नीतियों से कतई मेल नहीं खाते। दरअसल, इस मौके पर जिस बड़े पैमाने पर सरकारों ने कमजोर तबकों की मदद और अर्थव्यवस्था को संभालने के उपाय किए हैं, वह पिछले चार दशक से अपनाई गई नीतियों के खिलाफ जाते हैं। इन नीतियों को समग्र रूप से नव-उदारवाद कहा जाता है। इस विचार का दौर अमेरिका में रोनाल्ड रेगन और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के सत्ता में आने का साथ शुरू हुआ था। सोवियत संघ के विखंडन के साथ ऐसा लगा कि इन नीतियों का अब कोई विकल्प नहीं है। यह कथन चल पड़ा कि- There is no alternative. इसका असर हुआ कि पहले वाम एवं जनतांत्रिक एजेंडे पर चलने वाली मुख्यधारा की ज्यादातर पार्टियां भी उस सोच का शिकार हो गईं- जिसे वाशिंगटन सहमति (consensus) के नाम से जाना गया है।
इस सोच को पहली चुनौती 2008 की आर्थिक मंदी के बाद ही मिलने लगी। जब इसके वैचारिक प्रणेताओं में रहे फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने विचार बदल लिए। अब कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच डोनल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन, इमैनुएल मैक्रों और अंगेला मार्कैल जैसे नव-उदारवादी शासक अपने-अपने देशों में जन-कल्याण एवं अर्थव्यवस्था को निर्देशित करने की कथित समाजवादी नीतियों पर चल पड़े हैं। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ वैश्विक पूंजी और ऩव-उदारवाद के सबसे मजबूत पैरोकारों में रहा है। वह ब्रिटिश कंजरवेटिव पार्टी का घोर समर्थक है। मगर बीते 3 अप्रैल को उसमें एक आलेख छपा, जिसका शीर्षक था- There is no alternative: we are all socialists now in the fight against corona virus. लाजिमी है कि इसे देख कर लोगों को हैरत हुई।
इसी अखबार की वेबसाइट पर पिछले दिनों ब्रिटिश लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू आया। उसमें यह सवाल सुनने को मिला कि जब पूंजीवाद को बचाने के लिए समाजवाद को अपनाया जा रहा है, तब आपको कैसा महसूस हो रहा है। गौरतलब है कि हाल में ब्रिटेन में समाजवादी राजनीति को फिर से खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान कॉर्बिन का ही रहा है। इसीलिए अब इन नीतियों को बहुत से लोग कॉर्बिन-वाद (Corbynism) भी कहते हैं। पिछले दिसंबर में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में कॉर्बिन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की करारी हार हुई। मगर कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच बदले माहौल में नेता पद से अपनी विदाई के पहले बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कॉर्बिन ने दावा किया कि ‘वे सही साबित हुए हैं।’ इस दावे किसी ने चुनौती नहीं दी।
वैसे वैश्विक पूंजी और नव-उदारवाद के मुखपत्र के रूप में द फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठा कहीं ज्यादा है। मगर 3 अप्रैल को इस अखबार ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया- Virus lays bare fraility of social contract. इसमें इसने कहा- “पिछले चार दशकों में अपनाई गई नीति-दिशा (policy direction) को पलटने के लिए आमूल सुधार लागू करना आवश्यक है। सरकारों को अर्थव्यवस्था में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सार्वजनिक सेवाओं को बोझ के बजाय उन्हें निवेश के रूप में देखना होगा। ऐसे उपाय करने होंगे जिससे श्रम बाजार की असुरक्षा घटे। पुनर्वितरण (Redistribution) फिर से एजेंडे पर आएगा और बड़े एवं धनी लोगों के विशेषाधिकारों पर सवाल खड़े किए जाएंगे। बुनियादी आय एवं वेल्थ टैक्स (धन कर) जैसी जिन ऩीतियों को अब तक विचित्र समझा जाता था, उन्हें अमल में लाना होगा।” जब फाइनेंशियल टाइम्स ऐसी बात कहने लगे तो क्या जेरमी कॉर्बिन के दावे में कोई बड़बोलापन देखा जा सकता है? क्या द फाइनेंशियल टाइम्स की टिप्पणी यह नहीं बताती कि आज दुनिया में किस तरह के विचार प्रभावशाली हो रहे हैं?
जो भूमिका कॉर्बिन ने ब्रिटेन में निभाई, वैसी रोल अमेरिका में बर्नी सैंडर्स ने निभाया है। सैंडर्स खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। अमेरिका में कभी सोशलिस्ट और अपराधी शब्द समानार्थी बताए जाते थे। वहां खुद को सोशलिस्ट कहते हुए एक बड़ा जनाधार बना लेना और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर देना एक चमत्कार-सा ही है। सैंडर्स ऐसा कर पाए, तो इसलिए पिछले दस साल में दुनिया में परिस्थितियां बदली हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐस्टैबलिशमेंट की तिकड़मों के कारण 2016 की तरह वे इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। मगर कोरोना वायरस से बने माहौल के बीच उनके विरोधी रहे- अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस के अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने पिछले 26 मार्च को एक लेख छापा, जिसका शीर्षक था- The corona virus shows Bernie Sanders won. उदारवादी पत्रिका द न्यूयॉर्कर ने एक विश्लेषण छापा- जिसका शीर्षक था कि वास्तविकता ने बर्नी सैंडर्स का समर्थन कर दिया है। बर्नी का एक प्रमुख मुद्दा मेडिकेयर पर फॉर ऑल यानी सबके लिए मुफ्त चिकित्सा का रहा है। कोरोना संकट ने इस मुद्दे की प्रासंगिकता सबके सामने स्पष्ट कर दी है।
हकीकत यही है कि दशकों से चल रही नव-उदारवादी नीतियों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अधिकांश देशों में उपेक्षा की गई। अतः अमेरिका में विशेषज्ञ यह कहने में कोई कोताही नहीं कर रहे कि वहां कोरोना की आफत नव-उदारवाद का परिणाम है। नियमों-विनियमों को खत्म करने, सरकार की भूमिका घटाने, मुनाफे के मकसद को समाज के अधिक से अधिक क्षेत्रों पर हावी होने देने आदि जैसी नीतियों का नतीजा है कि आज जब महामारी आई, तो सबसे धनी देशों में भी अस्पताल, डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी असहाय अवस्था में पाए गए। चमकदार, ऊंचे-ऊंचे प्राइवेट अस्पतालों की ऐसी महामारी में कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए स्पेन में इन अस्पतालों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। स्पेन में अभी समाजवादी पार्टी की सरकार है, जिसमें नव-समाजवादी यूनिदास पोदेमॉस भी शामिल है। मगर स्पेन पिछले दशकों में अपनाई गई नीतियों की कीमत चुका रहा है।
ऐसी ही कीमत इटली ने चुकाई है। वहां पिछले ढाई दशकों में ज्यादातर समय धुर दक्षिणपंथी, और विदेशी-आव्रजक विरोध के आधार पर अपनी राजनीति को संगठित करने वाली ताकतें सत्ता में रही हैं। सिल्वियो बर्लुस्कोनी से समय से आरंभ हुआ ये दौर अधिक से अधिक उग्र होता गया है। इसका नतीजा है कि देश में जनसंख्या का अंसतुलन पैदा हुआ। दूसरी तरफ सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर होती गईं। अतः जब महामारी पहुंची, तो इटली की सरकार के वश में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था।
तो तमाम पश्चिमी देशों की सरकारों ने इस संकट के समय सरकार की भूमिका बढ़ाई है। डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका में डिफेंस प्रोडक्शन ऐक्ट लागू कर दिया है, जिसके तहत सरकार को हर कंपनी को यह आदेश देने का अधिकार मिल गया है कि उसे क्या उत्पादन करना है। ऐसा अमेरिका में हो और वह भी ट्रंप प्रशासन करे, यह अभी एक महीना पहले सोचना असंभव था। बहरहाल, ऐसे अन्य कदम अन्य पूंजीवादी देशों में भी उठाए गए हैं। इसीलिए अब ये चर्चा आम है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से जब दुनिया उबरेगी, तब वह वैसी ही नहीं रह जाएगी, जैसी पहले थी। ग्लोबलाइजेशन का जो रूप था, वह मौजूद नहीं रहेगा। ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के तहत जो ग्लोबल सप्लाई चेन बना, उसने आज ये हाल बना दिया है कि सारी दुनिया में प्रमुख उत्पादन और वितरण आज ठप हैं। नव-उदारवाद ने समाज में विषमताएं बढ़ाई हैं और सरकारों को कमजोर किया है। उसका परिणाम महामारी का विकराल रूप ले लेना है। जबकि चीन, वियतनाम और स्कैंडेनेवियन आदि जैसे देशों ने- जहां पब्लिक सेक्टर मजबूत है, वहां इस समस्या का बेहतर ढंग से मुकाबला करने की मिसाल पेश की गई है।
तो यह तो आम समझ है कि कोरोना के बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी। मगर अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर ये कैसी बनेगी? बदलाव का रूप क्या होगा? क्या बर्नी सैंडर्स और जेरेमी कॉर्बिन ने जिन नीतियों की वकालत की है, उनका प्रभाव बढ़ेगा? क्या नियोजित अर्थव्यवस्था का दौर लौटेगा? या पूंजीवाद अपने सामने खड़े हुए विकट संकट से निकल जाएगा? यानी समाजवादी नीतियों का उपयोग पूंजीवाद को बचाने के लिए करने की मौजूदा मंशा कामयाब हो जाएगी और एक बार फिर दुनिया पर मुनाफे का पूंजीवादी तंत्र हावी हो जाएगा? इस बारे में अभी कुछ भी कहना शायद मुश्किल है।
इतिहास में जब कभी महामारियां आई हैं, उन्होंने अपना गहरा असर छोड़ा है। बाइबिल में कहा गया है कि युद्ध, अकाल, जंगली जानवर और प्लेग (यानी महामारी) आम जिंदगी को बदल डालते हैं। मगर बदलाव कैसा होगा, यह कभी पहले से तय नहीं होता। आज भी तय नहीं है। इसलिए इतिहास में ऐसी मिसालें हैं, जब तानाशाहों और जनता को गुमराह करने वाले नेताओं ने महामारियों या ऐसे संकटों से बने का माहौल का फायदा उठा लिया। यह पहलू अपने देश के लिए प्रासंगिक है। यह स्पष्ट है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, नव-उदारवाद और आर्थिक गैरबराबरी को लेकर कोई बहस खड़ी नहीं हुई है। दूसरी तरफ सत्ताधारी जमात कोरोना संकट को सांप्रदायिक रंग देने में सफल हो गया है, जो उसकी राजनीतिक सत्ता की सबसे बड़ी ताकत है। विपक्ष और उदारवादी जमातें महज सत्ताधारी दल द्वारा तय किए गए एजेंडे पर खेलने और प्रतिक्रिया जताने से अधिक कुछ करने में सक्षम नहीं दिखते। ऐसे में कोरोना बाद के समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में भले कुछ सकारात्मक और प्रगतिशील घटनाक्रम देखने को मिलें, मगर अपने यहां तो उम्मीद कोई ज्यादा उज्ज्वल नहीं दिखती।